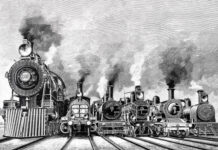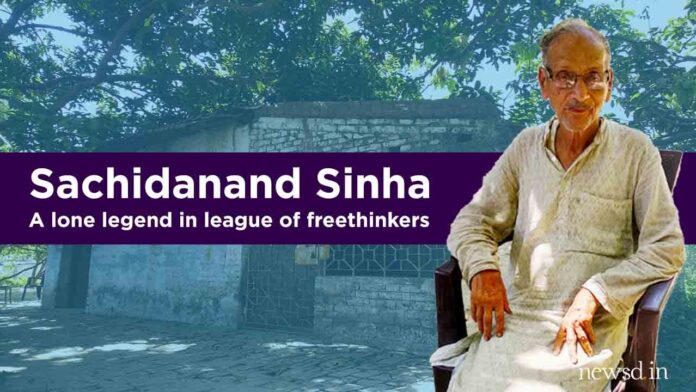समाजवादी चिंतक और लेखक सच्चिदानंद सिन्हा देश के उन विरले लोगों में हैं, जो सिद्धांतों को जीते हैं, सादगी और शालीनता ऐसी कि आज भी वह मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के गांव मनिका में छोटे से घर में अकेले रहते हैं।
उन्होंने शादी नहीं की, जीवन समाजवादी विचारधारा के प्रचार-प्रसार और मानवीय मूल्यों को समाज में स्थापित करने के संघर्ष में खपा दिया। सच्चिदानंद जी ने (30 अगस्त को) अपने जीवन के 94 साल पूरे कर लिये। उपभोक्तावाद के इस दौर में पद व शोहरत की लालसा के पीछे भागती एक पूरी पीढ़ी को 94 साल के इस मनीषी के बारे में जानना चाहिए, जो आज भी मानवीय मूल्यों को समाज में प्रतिष्ठापित करने की लड़ाई में एक लौ की तरह हैं। रजनीश उपाध्याय की बातचीत-
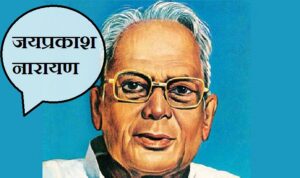
समाजवाद से जुड़ाव : दरअसल समाजवादी आंदोलन से मेरा जुड़ाव एकाएक नहीं हुआ। इसे समझने के लिए मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मेरे जीवन को देखना होगा. ननिहाल और मेरा परिवार आजादी की लड़ाई से जुड़ा था। पूरी बात तो याद नहीं, लेकिन धुंधली सी तस्वीर जेहन में है, जब मैं सिर्फ छह साल का थां, तो मेरे नाना को पकड़ने के लिए पुलिस आयी।
तब मैं मुंगेर में नाना के घर था. वह गांधीवादी और कांग्रेस के नेता थे। पुलिस घर का सारा सामान उठा ले गयी, यहां तक कि बर्तन भी। मैं और मेरे मामा छुप कर यह सब देख रहे थे। इसका मेरे मन मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव पड़ा, मेरे पिताजी कॉलेजियट स्कूल (मुजफ्फरपुर) में शिक्षक थे। उन्होंने बाद में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया तो मेरे नानाजी और पिताजी के संघर्ष का प्रभाव मुझ पर पड़ा। 1942 के आंदोलन के वक्त हमारी उम्र 13-14 साल की थी। नौवीं कक्षा का छात्र था।
तब तक मैंने चरखा से सूत काटने की कला सीख ली थी। पिताजी खादी की ट्रेनिंग देने वाले शिक्षक थे। मैं महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग भी देने लगा था, 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी आये थे. तो मैंने सूत काटकर उन तक पहुंचाया। तब तक गांधी जी से नजदीक से नहीं मिल पाया, इसके पहले नेहरू जी पटना आये, तो उनको भी सूत दिया. आजादी की लड़ाई के दौरान ही जेपी से प्रभावित रहा।

पढ़ाई लिखाई : मेरी स्कूलिंग कोई खास नहीं रही, शुरू में तो जैसे तैसे पढ़ाई हुई। 1940 में पहली बार सातवीं कक्षा में एडमिशन हुआ. पिताजी ने नौकरी छोड़ दी तो चाचा की देखरेख में रहा. सदाकत आश्रम में स्कूल खुला तो वहां मेरा एडमिशन हुआ। हॉस्टल में भी रहा, मैट्रिक पास करने के बाद 1945 में साइंस कालेज, पटना में एडमिशन हुआ। इसी दौरान मैं कांग्रेस से जुड़ गया, 1946 में सोशलिस्ट कांग्रेसमैन एसोसिएशन से जुड़ा, आइएससी की परीक्षा सेकंड डिवीजन से पास किया। बीएससी की पढ़ाई तक तो समाजवादी आंदोलन में भागीदारी बढ़ गयी तो पढ़ाई बाधित हुई।
जेपी-लोहिया का असर : देखिए, मैं तो मानता हूं कि जेपी खुद मार्क्सवादी थे। वह अमेरिका में पढ़े लिखे थे और मार्क्स का उन पर बड़ा प्रभाव था। जब वह भारत आये तो उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक लाइन लिया- डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन का, उनके साथ बड़ी संख्या में मेरे जैसे यूथ जुड़े, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1947 मे सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ,
तब की दुनिया की परिस्थिति का भी इन सब पर चीजों पर असर रहा। रूस में कम्युनिस्ट सरकार थी, लेकिन तानाशाही आ चुकी थी। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी. इससे समाजवादियों को बड़ा बल मिला। ब्रिटेन में ढांचा के भीतर परिवर्तन किया गया था। 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ तो सोशलिस्ट पार्टी को धक्का सा लगा। बाद का दौर सबको पता है, समाजवादियों में एकजुटता हुई।
टूट-फूट भी होती रही, 1953 में सोशलिस्ट पार्टी का विलय किसान मजदूर प्रजा पार्टी में हो गया, जिसका गठन कृपालानी जी ने किया था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी। तब के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि समाजवादियों का जवाहर लाल नेहरू के प्रति एक खास तरह का सॉफ्टनेस था, लेकिन, डॉ. राम मनोहर लोहिया नेहरू के कट्टर आलोचक थे। 1956 में लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। मेरा मानना है कि लोहिया काफी रैडिकल थे।
यह बात उनके भाषणों और आचार व्यवहार में भी देखी जा सकती थी। इस बात को समझना होगा कि 1974 का जो जेपी आंदोलन छात्रों का आंदोलन था। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट मूवमेंट था, वह समाजवादी आंदोलन नहीं था। छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जेपी बाद में आये थे। नक्सली आंदोलन : हमारा शुरू से लोकतांत्रिक समाजवाद में भरोसा रहा है, इतिहास गवाह है कि हिंसक राजनीति अंतत: हिटलरवाद की ओर जाता है। आज दुनिया भर में नजर डालें तो यह बात सही लगती है, अब चीन को देखिए, क्या हुआ वहां? क्रांति हुई, लेकिन आज चीन में फिर से पूंजीवाद आ गया। रूस की स्थिति देखिए। आदमी को जरूरत कम कर प्रकृति के पास जाना चाहिए. भारत की स्थिति यूरोप की तरह नहीं रही है। भारत में सामंती व्यवस्था का आधार जाति व्यवस्था रही है।
हमलोगों ने जाति के सवाल को हल नहीं किया। नक्सली संगठनो ने जहां-जहां भूमि आंदोलन चलाया, वहां जाति संघर्ष आगे आ गया। सबसे पहले जाति व्यवस्था को तोड़ना होगा, लोहिया ने इस बात को समझा था और उन्होंने तीन सूत्री एजेंडा दिया था। उन्होंने सहभोज का अभियान चलाया था, जिसमें सभी जाति के लोग एक साथ भोजन करें। उन्होंने अंतरजातीय विवाह की बात कही थी. कम्युनिस्ट पार्टियों ने जाति संघर्ष को हल नहीं किया।
सभ्यता का संकट : जिन विचारों को पहले खारिज किया जाता रहा, अब वे प्रासंगिक दिखाई दे रही हैं, अब लगता है कि हमलोग गलत दिशा में बढ़ रहे थे। सारे अनुभवों को देखने के बाद लगता है कि ऐसे समाज के निर्माण की ओर बढ़ना होगा, जो प्रकृति की ओर ले जाये. विकास की जो दिशा थी, वह एक तरफा थी। अब नये सिरे से सब कुछ की तलाश करनी होगी।
यह काम मुश्किल है. शायद 200 साल पहले उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जीवन बदल चुका है. लेकिन, कुछ इंडीकेटर बता रहा कि सभ्यता का संकट है और आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। यदि यह रास्ता मौत की तरफ जानेवाला है तो इसे बदलना ही होगा. जंगल खत्म हो रहा है, पर्यावरण का संकट बढ़ रहा है. जीवन का आधार रहीं नदियां नष्ट हो रहीं। तेल जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं। आधुनिक जीवन पद्धति अपने आप में संकट की जनक है. गैस पर खाना बनाते हैं, धुआं नहीं निकलता है।
लेकिन जहां से गैस निकाला जाता है, वह पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है. बिजली हमें राहत देती है, लेकिन जहां बिजली उत्पादन हो रहा है, वहां कोयला जलने से क्या हालत हो रही है. हमलोग इन सब चीजों के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, यह बड़ा सवाल है. जर्मनी वगैरह मे तो कोल आधारित उद्योग खत्म कर दिया गया है, लेकिन अपने देश में रैडिकल डिसिजन लेना होगा. यह जीवन का सवाल है तो कुछ तो सोचना होगा। कुछ सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा।
फिजिक्स की एक थ्योरी है- इन्ट्रोपी मतलब सम ताप। अधिक ताप कम ताप की ओर संक्रमण करता है। एक समय ऐसा भी आयेगा जब यह प्रक्रिया रुक जायेगी, स्थिर हो जायेगा।
तब समताप, मतलब न अधिक ताप होगा और न वह कम ताप की ओर संक्रमण कर पायेगी, यह प्रकृति और जीवन के नष्ट हो जाने की स्थिति होगी। इससे तो बचने का उपाय ढूंढ़ना ही होगा। समाजवाद का भविष्य : मैंने हाल के दिनों में अध्ययन की कोशिश की है. चीन में माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई, सांस्कृतिक क्रांति भी हुई लेकिन अब वह पूंजीवाद की तरफ चला गया। यूरोप के भीतर क्रांति प्रतिक्रांति हो गयी। रूस विघटन के बाद पूंजीवाद की तरफ बढ़ा। मुझे लगता है कि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था इन सबके मूल में है. औद्योगिक व्यवस्था शुरू से प्रकृति और मानव विरोधी रही है। इसके भीतर आप समतामूलक समाज बना ही नहीं सकते हैं. धातु पूरे सभ्यता का आधार रहा है।
इसकी खोज सभ्यता के विकास का एक टर्निंग प्वाइंट था, अब देखिए कि बॉक्साइट या दूसरे खनिज के लिए जहां भी माइनिंग हुआ या हो रहा है, वहां परिवेश नष्ट किया गया या हो रहा है, जहां भी माइनिंग होगा, वहां विस्थापन होगा. हर जगह प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। ऐसे में समता मूलक समाज बनाने की बात मौजूदा व्यवस्था में तो कारगर नहीं दिखती. लोगों को क्यूबा के प्रयोग से सीखना चाहिए। क्यूबा ने सहकारिता फार्म विकसित किया है। विशालता के तंत्र का त्याग करते हुए क्यूबा ने लघु इकाइयों के आधार पर अपनी व्यवस्था बनायी। पेस्टीसाइड के लिए उन लोगों ने प्राकृतिक चीजों का प्रयोग किया. ट्रैक्टर की जगह बैल से खेती शुरू की।
एकमात्र देश है, जो मॉडल है, मुझे लगता है कि गांधी आज ज्यादा प्रासंगिक हैं और यदि कोई मानवीय समाज बनाना है तो गांधी के रास्ते पर लौटना होगा और छोटे ग्रामीण गणराज्य पर सोचना होगा. ऐसे समाज की ओर बढ़ना होगा जो हमें प्रकृति की तरफ ले जाये. समाजवाद का भविष्य इसी में है।
गांधी की प्रासंगिकता : अब सब कुछ देखने पर लगता है कि महात्मा गांधी की प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा है, जब हमें मानवीय समाज बनाना है तो हमें छोटी इकाइयों के आधार पर व्यवस्था बनानी होगी। मशीन का निर्माण समाज ने किया, लेकिन मशीन ही संचालित करने लगी है। हमें ग्रामीण गणराज्य की ओर बढ़ना होगा। शुरू में तो हम भी (समाजवादी धारा के लोग) गांधी जी के काफी आलोचक रहे थे। गांधी जी ने अपने जीवन से भी मानक बनाया. जब भी उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने प्रयोग भी किया।
एक बार अफ्रीका में आंदोलन के दौरान जब लोग जेल चले गये तो उनके परिवार के सामने दिक्कत आयी कि कहां रहे। उनके एक मित्र ने 1100 एकड़ का फॉर्म जोहानिसबर्ग के पास दे दिया, सभी धर्मों के लिए वहां अलग-अलग किचेन बना, लेकिन गांधी जी ने कहा कि सबका खाना एक साथ बनेगा. तो एक तरह से कम्यून बन गया। शौचालय को लेकर भी उन्होंने प्रयोग किया था।
सच्चिदानंद सिन्हा ने करीब दो दर्जन पुस्तकें लिखी हैं, इनमें 10 अंग्रेजी में हैं
हिंदी में
समाजवाद के बढ़ते चरण :
नक्सलवाद का वैचारिक संकट
जिंदगी सभ्यता के हाशिए पर
भारतीय राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता
भारत में तानाशाही
मानव सभ्यता और राष्ट्र-राज्य
उपभोक्तावादी संस्कृति का जाल
संस्कृति और समाजवाद
भूमंडलीकरण की चुनौतियां
संस्कृति-विमर्श,
पूंजीवाद का पतझड़
जाति व्यवस्था : मिथक, वास्तविकता और चुनौतियां
लोकतंत्र की चुनौतियां
पूंजी का अंतिम अध्याय
वर्तमान विकास की सीमाएं
गुलाम मानसिकता की अफीम
अंग्रेजी में
द इंटरनल कॉलोनी
सोशलिज्म एंड पावर
इमरजेंसी इन पर्सपेक्टिव
द परमानेंट क्राइसिस इन इंडिया
द कास्ट सिस्टम
एडवेंचर एंड लिबर्टी
द बिटर हार्वेस्ट
कॉआलिशन इंन पॉलिटिक्स : (राजकमल प्रकाशन जल्द ही सच्चिदानंद सिन्हा रचनावली प्रकाशित करने वाला है. क्यूबा के प्रयोग पर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने लिखना शुरू किया था. लेकिन, बढ़ती उम्र और बीमारी की वजह से यह कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया.)
नैतिकता का सवाल : नैतिकता तो जीवन के अनुभव से ही पैदा होती है. आज जिसे हम नैतिकता कहते हैं, वह भी एक समाज मे खास परिस्थिति में जो संकट पैदा हुआ था, उससे उबरने के लिए नैतिक मूल्य अपनाये गये. आज के समाज में कुछ अलग मूल्य हैं.
राजनीतिक दलों की प्रासंगिकता : भारतीय लोकतंत्र बड़ा है. इसमें कही न कहीं ऐसी व्यवस्था होगी, जो लोगों की समस्याएं सत्ता तक पहुंचाये, स्वार्थ अलग अलग हैं. जातियों का, वर्ग का. राजनीति के केंद्र में लाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था तो रहेगी. दल एक तरह से रास्ता देती है, जिसके जरिये आप शिकायतों को ला सकें. समस्याओं को सत्ता तक पहुंचाने के माध्यम ये राजनीतिक दल ही हैं. दल तो रहेंगे. इनसे निजात नहीं पा सकते. राजनीतिक पार्टियां भी एक छोटा मॉडल हैं, उसमें समाज रिफ्लेक्ट होता है.
विषमताएं, अंतरविरोध. समाज के भीतर नयी पार्टियां बनती हैं, कुछ आदर्श को लेकर. लेकिन जो संघर्ष होता है, उसमें जो संगठित समूह होता है, वे ज्यादा सफल हो जाते हैं. सबका हित नहीं हो पाता। विशाल समाज में पार्टियां अनिवार्य हैं. उसमें बुराई भी दिखेगी, क्योंकि उसके नेता कोई देवदूत तो हैं नहीं. वे भी समाज से आते हैं, गांधीजी के विचार प्रासंगिक इसमें भी दिखते हैं। छोटे समाज की कल्पना करनी होगी, गांधी जी छोटी व्यवस्थाओं की बात करते थे. यही हो सकता है।
विकास का मॉडल : मेरे दिमाग में तो एक बात आती है कि तकनीक के विकास की वजह से विज्ञान की जो दिशा थी, शायद कुछ गलत थी. कभी कभी हम सोचते हैं कि जो बिजली जलाते हैं, कोयला है।
क्या विज्ञान ऐसा करता कि जुगनू से जो प्रकाश मिलता है, उस तरह का कोई विज्ञान विकसित कर सकते थे. जैसे चीनी गन्ना से विकसित होता है, लेकिन मधुमक्खियां भी तो मिठास पैदा करती हैं तो क्या विज्ञान की दिशा गलत थी और अब हम लोग उससे कुछ अलग कर सकते हैं, इस पर सोचना होगा।