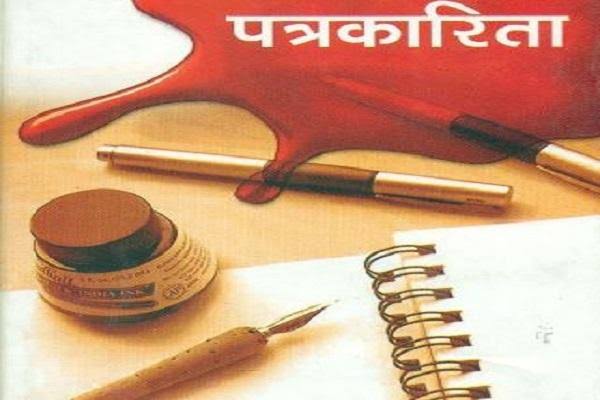पत्रकारिता का यह मिशन आजादी के बाद के तीन दशकों तक भी इसी जुझारू प्रण से चलता रहा 1947 से लेकर 1977 तक के इस दौर में पत्रकारों की पैनी कल ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों को भी नहीं बख्शा। मामला चाहे रक्षा मंत्रालय में जीप घोटाले का हो या फिर चीन के साथ युद्ध में भारत की पराजय का, बंगाल का दुर्भिक्ष हो या फिर देश में आपातकाल लगाने का या फिर पूर्वोत्तर समेत अशांत हिमालयी राज्यों में विदेशी घुसपैठ का, हर मोर्चे पर मीडिया ने सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया था। आपातकाल की घोषणा के विरोध में तो देश के कई अखबारों ने कई दिन तक संपादकीय ही नहीं लिखे, सम्पादकीय का नियत स्थान काले बाॅर्डर के साथ खाली छोड़ दिया गया था। आज उस दृश्य की केवल परिकल्पना ही की जा सकती है, आज की पीढ़ी तो इसे कपोल कल्पना ही समझती है।
हमारे देश की पत्रकारिता के इतिहास, स्वरूप में आये बदलाव और मूल्यों के सत्यानाश होने की परिस्थितियों को देख कर ऐसा लगता है कि यहां की पत्रकारिता में राजनीति का असर हमेशा ही ज्यादा रहा है। जैसे-जैसे राजनीति बदली वैसे-वैसे ही मीडिया का स्वाभाव और स्वरूप भी बदलता गया। 1989 से भारतीय राजनीति में मंदिर बनाम मस्जिद के विवाद का सिलसिला शुरू हुआ, तो मंदी भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इसी दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री काल में मंडल के नाम पर चलायी गयी राजनीति ने पत्रकार जगत को मंदिर बनाम मस्जिद के साथ ही आरक्षण बनाम गैर-आारक्षण के खेमों में बांट दिया तभी से यह विभाजन रेखा चली ही आ रही है। इसी को मंडल बनाम कमंडल की राजनीति भी कहा जाता है।
आज की पत्रकारिता का खोखलापन इस रूप में भी देखा जा सकता है कि हम खबरों की खरीदारी भी बड़ी आसानी से करने लगे हैं, और इस मामले में प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सभी के बारे में इसी जुमले का इस्तेमाल किया जा सकता है कि हमाम में सारे ही नंगे हैं, कुछ अपवादों को छोड़ कर। इन हालातों में सामाजिक सरोकार की अनदेखी होना स्वाभाविक ही है। उस पर संपादक विहीन सोशल मीडिया ने हालत और खराब कर दी है। कुल मिला कर परिस्थिति इतनी नाजुक हो गयी है, कि न कुछ निगलते बनता है न थूकते।