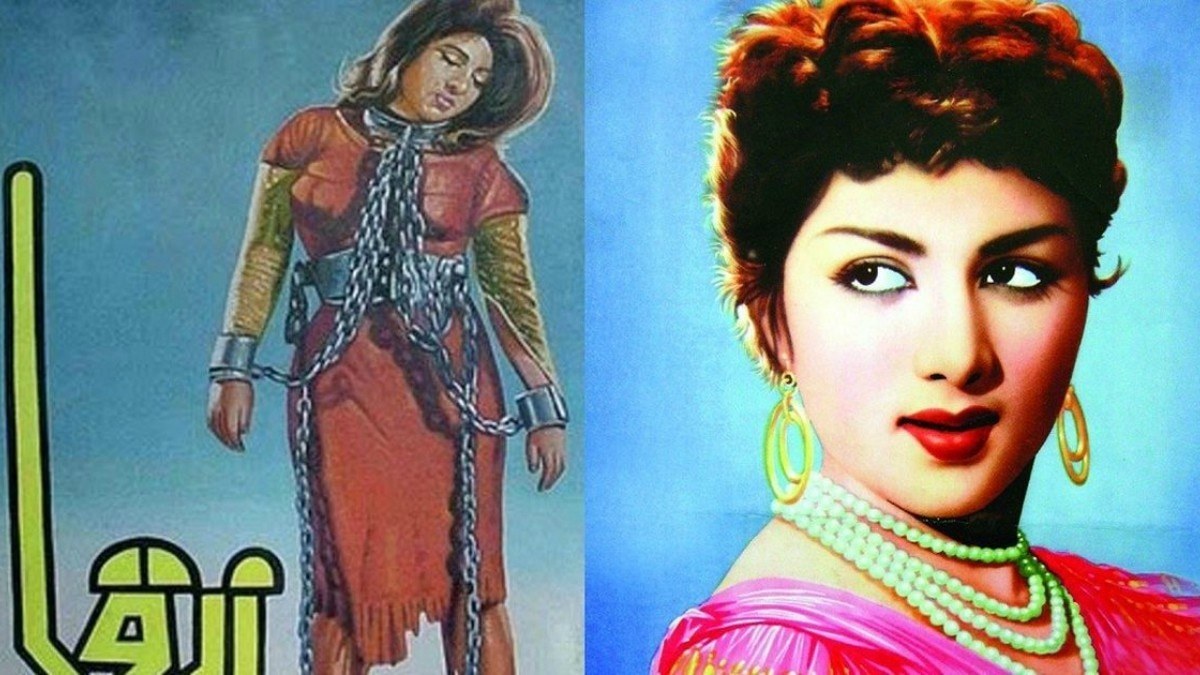अनिल जैन
एक साल से कुछ ज्यादा दिन तक चले किसान आंदोलन ने केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों के बहुआयामी दमनचक्र का जिस शिद्दत से मुकाबला करते हुए उन्हें अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर किया है, वह अपने आप में ऐतिहासिक है और साथ ही केंद्र सरकार के तुगलकी फैसलों से आहत समाज के दूसरे वर्गों के लिए एक प्रेरक मिसाल भी। इस आंदोलन ने साबित किया है कि जब किसी संगठित और संकल्पित आंदोलित समूह का मकसद साफ हो, उसके नेतृत्व में चारित्रिक बल हो और आंदोलनकारियों में धीरज हो तो उसके सामने सत्ता को अपने कदम पीछे खींचने ही पड़ते हैं, खास कर ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, जिनमें वोटों के खोने का डर किसी भी सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व के मन में सिहरन पैदा कर देता है। देश की खेती-किसानी से संबंधित तीन विवादास्पद कानूनों का रद्द होना बताता है कि देश की किसान शक्ति ने सरकार के मन में यह डर पैदा करने में कामयाबी हासिल की है।
किसानों के इस ऐतिहासिक आंदोलन के चलते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करना और फिर किसानों की बाकी मांगों को भी मान लेना बताता है कि सरकार किसान आंदोलन से बुरी तरह डरी हुई थी। पिछले महीने विभिन्न राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की कुछ सीटों के लिए उपचुनाव के नतीजों को देख कर प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। उन्हें उम्मीद थी कि उनके इस ऐलान के बाद किसान अपना आंदोलन खत्म कर अपने-अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
किसानों ने तीन कानूनों की वापसी के ऐलान का तो स्वागत किया लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि वे सरकार की झांसेबाजी में फंसने को तैयार नहीं हैं। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी, बिजली कानून, किसानों पर कायम किए गए फर्जी मुकदमों की वापसी जैसे मुद्दों पर भी एक मुश्त फैसला चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सरकार को बता दिया कि जब तक उनकी बाकी मांगों पर भी फैसला नहीं होगा तब तक वे अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। इस बीच विधानसभा चुनाव वाले राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही प्रधानमंत्री की रैलियों में तमाम सरकारी संसाधन झोंक देने के बावजूद अपेक्षित भीड़ नहीं जुट पाने और विपक्षी दलों की रैलियों में उमड़ रही स्वस्फूर्त भीड़ ने भाजपा को उसकी राजनीतिक जमीन खिसकने का अहसास करा दिया। इसी अहसास ने ‘मजबूत’ सरकार को किसानों की बाकी मांगे मानने के लिए भी मजबूर कर दिया।
इस किसान आंदोलन ने याद दिलाया है कि संसद जब आवारा या बदचलन होने लगती है तो सड़क उस पर अंकुश लगाने और उसे सही रास्ता दिखाने का काम करती है। किसानों की यह जीत न सिर्फ सरकार के खिलाफ बल्कि कॉरपोरेट घरानों की सर्वग्रासी और बेलगाम हवस के खिलाफ भी एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल होने का क्षण है, जिसके दूरगामी प्रभाव अवश्यम्भावी है। यह जीत रेलवे, दूरसंचार, बैंक, बीमा आदि तमाम सार्वजनिक और संगठित क्षेत्र के उन कामगार संगठनों के लिए एक शानदार नजीर और सबक है, जो प्रतिरोध की भाषा तो खूब बोलते हैं लेकिन कॉरपोरेट के शैतानी इरादों से लड़ने और उनके सामने चट्टान की तरह अड़ने का साहस और धैर्य नहीं दिखा पाते हैं। उनकी इसी कमजोरी की वजह से सरकार एक के बाद एक सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम उपक्रम अपने चहते कॉरपोरेट महाप्रभुओं के हवाले करती जा रही है।
पिछले साल संविधान दिवस (26 नवंबर) से शुरू हुआ और इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (10 दिसंबर) पर स्थगित हुआ किसानों का यह आंदोलन दुनिया के इतिहास में संभवत: इतना लंबा चलने वाला पहला ऐसा आंदोलन है, जो हर तरह की सरकारी और सरकार प्रायोजित गैर सरकारी हिंसा का सामने करते हुए भी पूरी तरह अहिंसक बना रहा। हालांकि इसको हिंसक बनाने के लिए सरकार की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। तमाम तरह से उकसावे की कार्रवाई हुई है, लेकिन आंदोलनकारियों ने गांधी के सत्याग्रह का रास्ता नहीं छोड़ा है। यही नहीं, इस आंदोलन ने सांप्रदायिक और जातीय भाईचारे की भी अद्भूत मिसाल कायम की है, जिसे तोड़ने की सरकार की तमाम कोशिशें भी नाकाम रही हैं।
यह सब चलता रहा और इस दौरान ठंड, गरमी, बरसात और कोरोना महामारी का सामना करते हुए आंदोलन स्थलों पर करीब 800 किसानों की मौत हो गई। सरकार के मंत्री और सत्तारूढ़ दल के नेता उन किसानों की मौत को लेकर भी निष्ठुर बयान देते रहे, खिल्ली उड़ाते रहे। इसी के साथ सरकार की ओर से यह बात भी लगातार दोहराई जाती रही कि कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं लिए जाएंगे।
सरकार की मगरुरी और उसके दमनचक्र का मुकाबला करते हुए संगठित और संकल्पित किसानों ने नजीर पेश की कि मौजूदा दौर में नव औपनिवेशिक शक्तियों से अपने हितों की, अपनी भावी पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिये कैसे जूझा जाता है। उन्हें अच्छी तरह अहसास है कि अगर कॉरपोरेट और सत्ता के षड्यंत्रों का डट कर प्रतिकार नहीं गया तो उनकी भावी पीढ़ियां हर तरह से गुलाम हो जाएंगी।
किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान सत्ता-शिखर के मन में जो डर पैदा किया है, वह डर निजीकरण की आंच में झुलस रहे सार्वजनिक क्षेत्र के आंदोलित कर्मचारी नहीं पैदा कर पाए हैं। इसकी वजह यह है कि सत्ता में बैठे लोग और उनके चहेते कॉरपोरेट घराने इन कर्मचारियों के पाखंड और भीरुता को अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि दिन में अपने दफ्तरों के बाहर या किसी चौक-चौराहे पर खडे होकर नारेबाजी करने वाली बाबुओं की यह जमात शाम को घर लौटने के बाद अपने-अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर सत्ताधारी दल के हिंदू-मुसलमान, मंदिर-मस्जिद, गाय-गोबर, श्मशान-कब्रस्तान, जिन्ना, पाकिस्तान जैसे तमाम प्रपंचों को हवा देने वाले व्हाट्सएप संदेशों, टीवी की चैनलों की बकवास या फूहड़ कॉमेडी शो में रम जाएगी।
”विकल्प क्या है’’ और ”मोदी नहीं तो कौन’’ जैसे सवालों का नियमित उच्चारण करने में आगे रहने वाले ये कर्मचारी अपने आंदोलन रूपी कर्मकांड से किसी भी तरह का डर सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व के मन नहीं जगा पाए हैं। यही हाल नोटबंदी और जीएसटी की मार से कराह रहे छोटे और मझौले कारोबारी तबके का भी है। इसे हम राजनीतिक फलक पर शहरी मध्य वर्ग के उस चारित्रिक पतन से भी जोड़ सकते हैं जो उन्हें उनके हितों से तो वंचित कर ही रहा है, उसकी भावी पीढ़ियों की जिंदगियों को दुश्वार करने का आधार भी तैयार कर रहा है। बहरहाल देश के श्रम कानूनों के दायरे में आने वाले संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को किसानों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन से डरी सरकार ने न सिर्फ किसानों की सभी मांगों को मंजूर किया है बल्कि उसी डर से वह श्रम सुधार के नाम पर बनाए गए नए श्रम कानूनों को भी अब टालने की तैयारी में है।