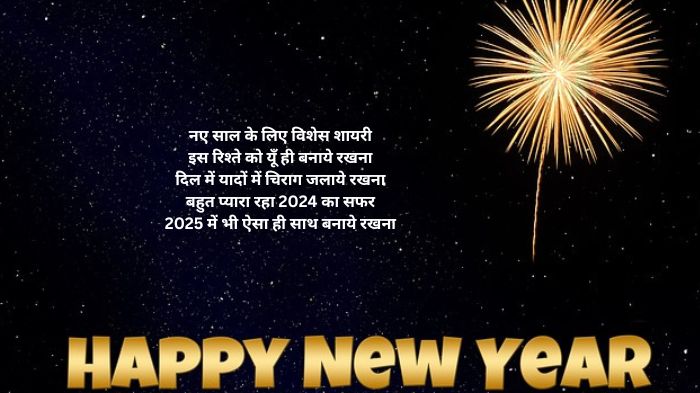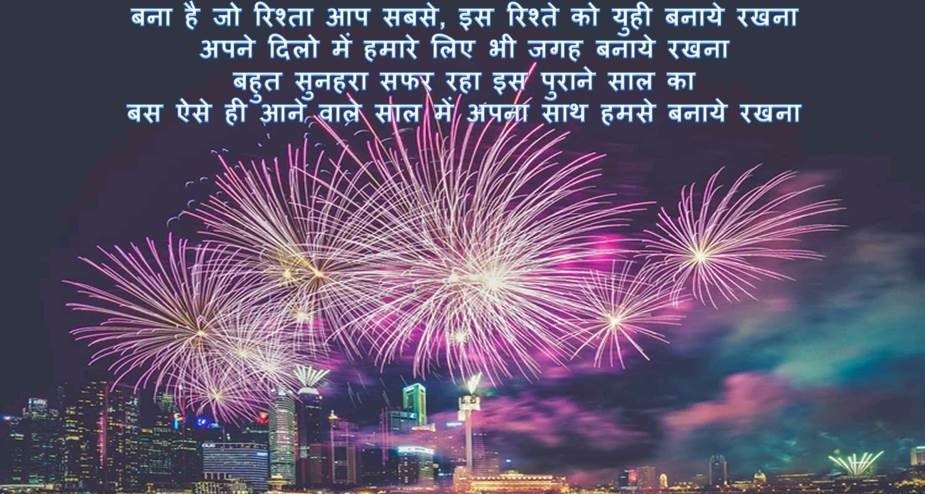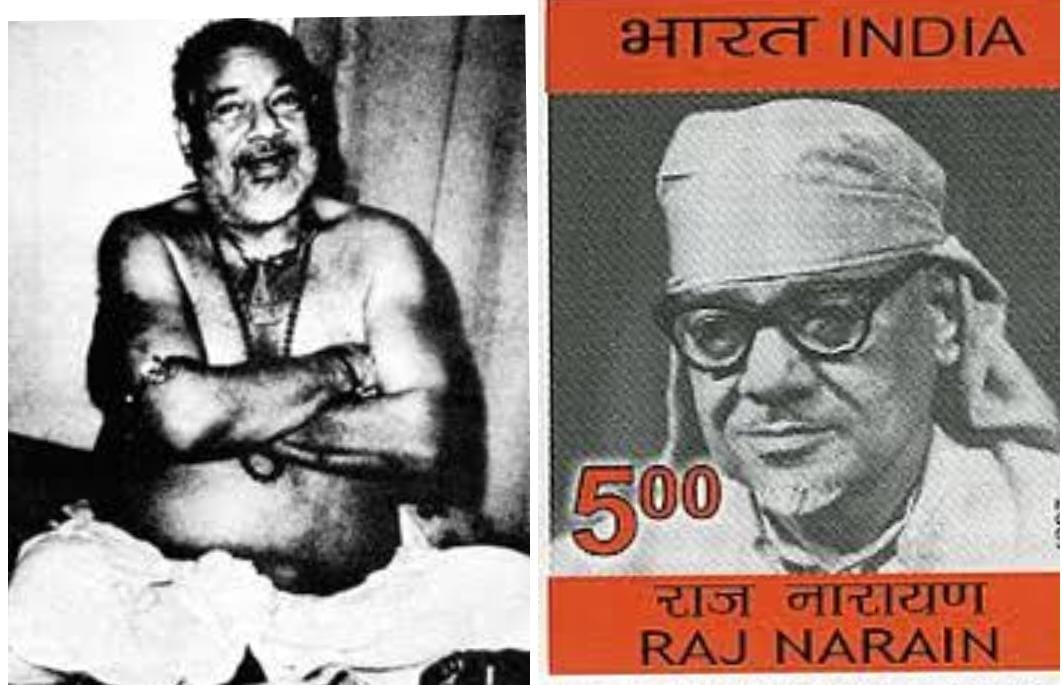निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ने से विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह बढ़ता है, जिससे रुपया कमजोर होता है। कच्चे तेल और सोने के बढ़ते आयात के कारण 2022 में भारत का रिकॉर्ड व्यापार घाटा रुपये के मूल्यह्रास को बढ़ाता है। भारतीय रुपये में गिरावट बाहरी क्षेत्र की कमज़ोरियों के बीच मुद्रा स्थिरता बनाए रखने की चुनौतियों को रेखांकित करती है। मुद्रा मूल्य में उतार-चढ़ाव वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और पूंजी बहिर्वाह के साथ-साथ राजकोषीय घाटे जैसे घरेलू कारकों से उत्पन्न होते हैं। भारत के बाहरी लचीलेपन को बढ़ाने और इसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय महत्त्वपूर्ण हैं।

डॉ. सत्यवान सौरभ
सितंबर 2024 के शेयर शिखर के बाद निरंतर बहिर्वाह ने रुपये को कमज़ोर कर दिया क्योंकि निवेशक अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि की अटकलों के बीच सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर चले गए। उच्च व्यापार घाटे जैसे व्यापार घाटे आयात पर बाहरी निर्भरता को उजागर करते हैं, विशेष रूप से ऊर्जा के लिए, रुपये की कमज़ोरी के दौरान चालू खाता घाटा बढ़ाते हैं। रुपये के अवमूल्यन के साथ भारत का कच्चे तेल का आयात बिल बढ़ गया, जिससे 2024 का व्यापार घाटा बढ़कर $75 बिलियन के करीब पहुँच गया।
टैरिफ़ की धमकियाँ और ब्रिक्स मुद्रा विवाद जैसी वैश्विक घटनाएँ भारत के बाहरी व्यापार और निवेश के लिए अनिश्चितताएँ पैदा करके अस्थिरता को बढ़ाती हैं। ब्रिक्स देशों की मुद्रा योजनाओं के खिलाफ़ अमेरिकी राष्ट्रपति की 2024 टैरिफ़ चेतावनी ने बाज़ार में बिकवाली को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की बाहरी स्थिरता कमज़ोर हुई। रुपये को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी निर्भरता निरंतर वैश्विक बाज़ार अशांति के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक लचीलेपन को प्रतिबंधित करती है।
रुपये को वापस 85.53 पर लाने के लिए दिसम्बर 2024 में एक ही तिमाही में $20 बिलियन से अधिक के भंडार को समाप्त कर दिया। कमज़ोर रुपया घरेलू मौद्रिक नीतियों को प्रतिबंधित करता है, महंगे आयातों के माध्यम से मुद्रास्फीति को बढ़ाता है जबकि विकास सम्बंधी चिंताओं को दूर करने के लिए राजकोषीय स्थान को कम करता है। दिसम्बर 2024 में कच्चे तेल के आयात की लागत 15% बढ़ गई, जिससे नीति निर्माताओं पर मुद्रा प्रबंधन और राजकोषीय विस्तार रणनीतियों को प्रभावी ढंग से संतुलित करने का दबाव पड़ा।
टैरिफ या प्रतिबंध जैसे संरक्षणवादी व्यापार उपाय, व्यापार संतुलन को बाधित करके मुद्रा स्थिरता को कमज़ोर कर सकते हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच राजनीतिक अस्थिरता या संघर्ष अस्थिरता पैदा करते हैं, जिससे सुरक्षित-पनाहगाह डॉलर की मांग बढ़ती है और उभरते बाजारों की मुद्राएँ कमज़ोर होती हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे भारत के आयात बिल पर दबाव पड़ा और रुपये का मूल्य कम हुआ। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सख्त मौद्रिक नीतियों के कारण भारत से पूंजी का बहिर्वाह होता है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है।
2022-23 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों में बढ़ोतरी के कारण विदेशी पोर्टफोलियो का बहिर्वाह हुआ, जिससे रुपया कमज़ोर हुआ।
निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ने से विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह बढ़ता है, जिससे रुपया कमजोर होता है। कच्चे तेल और सोने के बढ़ते आयात के कारण 2022 में भारत का रिकॉर्ड व्यापार घाटा रुपये के मूल्यह्रास को बढ़ाता है। उच्च घरेलू मुद्रास्फीति मुद्रा मूल्य को कम करती है, जिससे निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। कच्चे तेल जैसे अलोचदार आयातों की बढ़ती कीमतों ने भारत के आयात बिलों को बढ़ा दिया, जिससे 2023 में रुपया कमजोर हो गया। घरेलू और विदेशी निवेश में गिरावट कमजोर आर्थिक विकास का संकेत देती है, जिससे मुद्रा प्रवाह हतोत्साहित होता है। 2024 में, कॉर्पोरेट प्रदर्शन में कमी और स्टॉक वैल्यूएशन में वृद्धि के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बहिर्वाह हुआ। मुद्रा को स्थिर करने के लिए केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा सीमित हैं और केवल अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं। दिसम्बर 2024 में आरबीआई के देर से हस्तक्षेप ने रुपये को अस्थायी रूप से 85.53 प्रति डॉलर पर स्थिर करने में कामयाबी हासिल की। राजकोषीय रूप से विवश सरकार बाहरी झटकों को प्रबंधित करने की अपनी क्षमता को कम करती है, जिससे मुद्रा स्थिरता में विश्वास कमजोर होता है। महामारी के दौरान भारत के रिकॉर्ड राजकोषीय घाटे ने बाहरी लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपायों को सीमित कर दिया। मुद्रा नीतियों पर सरकार का स्पष्ट रुख निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और सट्टा दबाव कम करता है। आरबीआई गवर्नर द्वारा 2024 में डी-डॉलराइजेशन को खारिज करने से बाज़ार आश्वस्त हुआ, जिससे रुपये के मूल्यह्रास की चिंताएँ अस्थायी रूप से कम हो गईं। ।
बाह्य लचीलेपन को मज़बूत करने के उपाय हैं, निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने और व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए मूल्यवर्धित विनिर्माण और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना। फार्मास्यूटिकल्स और आईटी जैसे क्षेत्रों को मज़बूत करने से व्यापार घाटे को कम करने और रुपये को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। विविध आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक समझौते करके अस्थिर कच्चे तेल और आवश्यक आयात पर निर्भरता कम करें। रूस और मध्य पूर्वी देशों से कच्चे तेल के आयात का विस्तार करने से 2023 में औसत तेल आयात लागत कम हो गई। प्रभावी मुद्रा स्थिरीकरण के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड और सोने के संचय के माध्यम से मज़बूत भंडार बनाएँ।
रिज़र्व बैंक के अनुसार 2021 में $600 बिलियन के रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार ने महामारी के दौरान अस्थिरता को प्रबंधित करने में मदद की। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को निपटाने, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और विनिमय दर जोखिमों को कम करने के लिए समझौतों में शामिल हों। भारत-रूस रुपया-रूबल व्यापार तंत्र ने रूस-यूक्रेन संकट के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया। मुद्रा जोखिमों से बचने के लिए अल्पकालिक बाहरी ऋण को कम करते हुए कम लागत और लंबी अवधि के उधार को प्राथमिकता दें।
भारत द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने में वृद्धि ने 2023 में पुनर्भुगतान अस्थिरता को कम करने के साथ स्थिर विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद की। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के आर्थिक लचीलेपन के लिए एक मज़बूत बाहरी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है। निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति सुनिश्चित करके, विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाकर और रुपये में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर, भारत मुद्रा अस्थिरता को कम कर सकता है। संरचनात्मक सुधारों और वैश्विक आर्थिक एकीकरण पर ज़ोर देने वाली एक दूरदर्शी रणनीति दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मज़बूत करेगी।