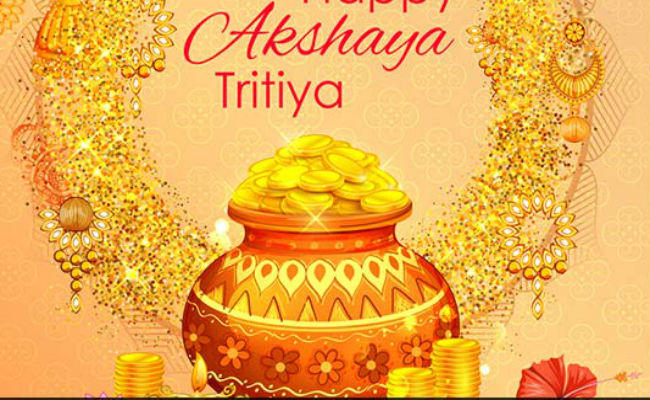“जिन हाथों ने इस देश की इमारतें खड़ी कीं, उन्हीं हाथों को आज रोटी, छत और पहचान के लिए जूझना पड़ रहा है। दिहाड़ीदार मजदूर केवल श्रम नहीं देते, वे इस देश की नींव हैं — लेकिन सबसे उपेक्षित भी। विकास की रफ्तार में उनका पसीना झलकता है, पर उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। क्या यही है ‘नए भारत’ का सपना — जहाँ श्रमिक अनदेखे, अनसुने और असुरक्षित रहें?”

डॉ. सत्यवान सौरभ
बदलते दौर में जब तकनीक, पूंजी और ग्लैमर की दुनिया भारत को चमकाता दिखता है, तब देश का एक बड़ा तबका ऐसा है जो उस चमक की नींव बनाता है लेकिन खुद अंधेरे में घुटता रहता है। यही तबका है — दिहाड़ीदार मजदूर। जिनकी बदौलत गगनचुंबी इमारतें खड़ी होती हैं, सड़कों पर रफ्तार दौड़ती है, और शहर सांस लेता है। परन्तु विडंबना यह है कि इन मजदूरों के जीवन में न तो स्थिरता है, न सुरक्षा, न पहचान और न ही संवेदनशीलता।
दिहाड़ीदार मजदूरों की दुर्दशा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक उपेक्षा और संस्थागत असफलताओं की भी उपज है। कोविड-19 महामारी हो या हालिया शहरी आपदाएँ, सबसे पहला और सबसे गहरा आघात इसी वर्ग को झेलना पड़ा। रोज कमाने-खाने वाले इन श्रमिकों के लिए लॉकडाउन और आर्थिक मंदी जीवन-मरण का प्रश्न बन गई। सरकारी घोषणाओं में इनके नाम भले दर्ज हों, पर न आंकड़ों में इनका कोई भरोसेमंद रिकॉर्ड है, न योजनाओं के क्रियान्वयन में इनकी प्राथमिकता।
भारत का श्रमबल लगभग 500 मिलियन है, जिसमें से 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। शहरी भारत की लगभग 72 प्रतिशत कार्यशक्ति दिहाड़ी श्रमिकों के रूप में काम कर रही है। यह “बैकएंड इंडिया”, जिसे कोई नहीं देखता, “फ्रंटएंड इंडिया” की रफ्तार बनाए रखने के लिए दिन-रात खटता है। यह वर्ग न केवल भारत की, बल्कि सिंगापुर, दुबई और खाड़ी देशों की आधुनिकता की नींव भी है। लेकिन विडंबना है कि इन्हें कोई पहचान पत्र नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई स्थायित्व नहीं — केवल मेहनत और उपेक्षा मिली है।
भारत में मजदूरों की लड़ाई कोई नई नहीं है। ब्रिटिश काल में बॉम्बे मिल मजदूर आंदोलन (गिरनी कामगार आंदोलन) से लेकर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना तक, मेहनतकशों ने संगठित होकर अपने हक की आवाज़ बुलंद की। 1 मई को ‘मजदूर दिवस’ के रूप में मनाने की परंपरा भले शिकागो आंदोलन से शुरू हुई हो, लेकिन भारत के श्रमिकों ने भी समय-समय पर सत्ता को झकझोरने वाला संघर्ष किया है। परंतु दुखद यह है कि 21वीं सदी में भी उनके मुद्दे वैसे ही हैं — न्यूनतम वेतन, सुरक्षा, और गरिमा।
फैक्ट्रियाँ, होटल, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन साइट्स, डिलीवरी सेवाएँ — सब इन पर निर्भर हैं। ओला-उबर ड्राइवर से लेकर राजमिस्त्री, बढ़ई, फूड डिलीवरी बॉय और प्लंबर तक — ये ही हैं जो शहरों को गतिशील बनाए रखते हैं। लेकिन जब सवाल उनके अधिकारों का आता है तो तंत्र मौन हो जाता है। इनके लिए न पर्याप्त जल-स्नान की व्यवस्था है, न सुरक्षित आवास, न शुद्ध पेयजल, न स्वास्थ्य सेवाएँ। हाथ धोने की सलाह दी जाती है, पर इनके लिए हैंडपंप भी अविश्वसनीय होते हैं। बीमार हों तो अस्पताल की कतार में कोई नाम नहीं, बैंक हो तो खाता नहीं, और श्रम हो तो मान्यता नहीं। संक्रमण, अस्वास्थ्यकर माहौल और मानसिक शोषण की तीनहरी मार इन पर हर रोज़ पड़ती है।
इन मेहनतकशों में बड़ी संख्या महिला श्रमिकों की है — निर्माण स्थलों पर ईंट ढोती, घरों में बर्तन माँजती, खेतों में पसीना बहाती, और फिर घर लौटकर चूल्हा-चौका भी संभालतीं। इनके पास न मातृत्व अवकाश है, न यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, न ही समान वेतन की गारंटी। सबसे दुखद यह है कि महिला मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अक्सर ‘अदृश्य’ मान लिया जाता है।
कोविड-19 महामारी के दौरान जब शहरों में लॉकडाउन लगा, तब सड़कों पर नंगे पांव, भूखे-प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल लौटते प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें पूरे देश को झकझोर गईं। जिन हाथों ने शहर बनाए, वे ही सबसे बेगाने हो गए। सरकारें एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालती रहीं, और ये मजदूर अपने गाँवों की ओर लौटते हुए ट्रेन की पटरी तक पर जान गंवाते रहे।
ऐसी स्थिति में सवाल उठता है — इनकी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? सरकारें जो केवल चुनावी मौसम में इन्हें याद करती हैं? समाज जो केवल इनके श्रम का उपयोग करता है पर इंसान नहीं समझता? या वह नीति-तंत्र जो अभी भी इन्हें “अस्थायी” मानता है, जबकि पूरा शहरी भारत इन्हीं के श्रम पर टिका है? हमारे शहर यदि किसी की हड्डियों पर खड़े हैं, तो क्या उनका हक़ सिर्फ पसीना बहाना है? क्या देश के विकास का मतलब सिर्फ ऊँची इमारतें हैं, या उन इमारतों को खड़ा करने वाले हाथों की खुशहाली भी?
हमें नीतिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर क्रांति की आवश्यकता है। सबसे पहले, इनके पंजीकरण की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए — “ई-श्रम पोर्टल” जैसी पहल को व्यापक और स्थानीय स्तर पर पहुँचाना होगा। साथ ही, “असंगठित कामगार सूचकांक नंबर कार्ड” को हर मजदूर तक पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता बननी चाहिए। यह न केवल उन्हें एक पहचान देगा बल्कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का जरिया भी बनेगा।
सामाजिक सुरक्षा कोष में तेजी लाना अब विलंब नहीं सह सकता। हर मजदूर को स्वास्थ्य बीमा, न्यूनतम वेतन की गारंटी, और आकस्मिक परिस्थितियों में राहत मिलनी ही चाहिए। स्मार्ट शहर की परिभाषा तब तक अधूरी है जब तक वह अपने सबसे असुरक्षित श्रमिक को गरिमा नहीं दे पाता। स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी चाहिए कि वे इन दिहाड़ीदारों को उनके कौशल के अनुसार रोज़गार से जोड़ने का काम करें। एक “श्रम सहायता केंद्र” हर नगर में हो, जो जानकारी, परामर्श, और सहायता का केंद्र बने।
भारत से सिंगापुर, कतर और दुबई जैसे देशों में गए मजदूरों की मेहनत वहाँ की इमारतों की पहचान बनी। लेकिन वहाँ भी उनके लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी, और यहाँ अपने देश में तो वे ‘कमजोर तबका’ कहलाते हुए पूरी तरह उपेक्षित हैं। विकासशील देश के नागरिकों को अपने ही देश में ‘दूसरे दर्जे’ का नागरिक बनाना कैसी विडंबना है?
गुरुग्राम के निर्माण स्थल पर काम करने वाले रामनाथ प्रतिदिन 12 घंटे ईंट-बजरी उठाते हैं। वे और उनकी पत्नी दोनों मजदूरी करते हैं, फिर भी बच्चों की स्कूल फीस देने में असमर्थ हैं। “हमने शहर को बनाया है, लेकिन शहर में रहने का हक़ हमारा नहीं,” वे कहते हैं। रामनाथ कोई अपवाद नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों मजदूरों की प्रतिनिधि आवाज़ हैं।
आज जब हम मजदूर दिवस मना रहे हैं, तब यह केवल प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए। यह दिन हमें यह सोचने पर विवश करे कि क्या हम वाकई अपने निर्माणकर्ताओं को वह सम्मान, वह सुरक्षा और वह जीवन दे पा रहे हैं, जिसके वे हक़दार हैं? यदि नहीं, तो इस देश के विकास की इमारत खंडहर में बदलने में समय नहीं लगेगा।
शहर की रफ्तार में जो साँसें लगी हैं,
वो थकती हैं पर रुकती नहीं हैं।
जिनके पसीने से सीमेंट सने हैं,
वही सबसे अनसुने हैं।
अब समय है कि हम केवल दीवारें न खड़ी करें,
बल्कि उन हाथों को पहचान दें जो उन्हें खड़ा करते हैं।